क्या एआई के चलते गूगल, क्वोरा और विकीपीडिया की भी नौकरी जा सकती है?
क्यों एआई के चलते सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि इंटरनेट के सबसे बड़े दिग्गज भी अपनी जगह खोने के डर से जूझ रहे हैं
जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नुकसानों की बात होती है, तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके चलते अपनी पारंपरिक नौकरियां खो देंगे. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसा होना शुरू भी हो चुका है.
लेकिन जिस बात पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वह यह है कि इस दौड़ में इंसान अकेला नहीं है. इंटरनेट को उसकी मौजूदा शक्ल देने वाले सबसे बड़े टेक दिग्गजों — गूगल, क्वोरा और विकीपीडिया — को भी अब एआई के चलते अपना धंधा छिन जाने का खतरा सता रहा है.
अब तक जब भी कोई सवाल होता तो हम गूगल से पूछा करते थे. कोई तथ्य चाहते, तो विकीपीडिया था. और अगर कोई व्यक्तिगत अनुभव या जानकारी जरूरी लगती, तो क्वोरा का सहारा था. ये प्लेटफॉर्म्स सालों से इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी पाने के सबसे लोकप्रिय ठिकाने रहे हैं.
लेकिन वह दौर अब बड़ी तेज़ी से और बिना किसी शोर-शराबे के खत्म होता जा रहा है.
आज जानकारी का एक नया तंत्र बन रहा है. एआई टूल्स — जैसे चैटजीपीटी, जैमिनी और क्लॉड — इसके केंद्र में हैं. और हैरानी की बात यह है कि जिस एआई क्रांति को कभी गूगल ने बढ़ावा दिया था, आज उसी ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है.
यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है, इंटरनेट पर जानकारी के बहाव का पूरा ढांचा ही खामोशी से उलट-पलट हो रहा है.
गूगल की बदलती भूमिका:
सालों तक गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं था. वह इंटरनेट की दुनिया का मेन गेट था. कोई भी सवाल टाइप करते और गूगल सिर्फ एक पल में हमारे सामने संभावित जवाबों की कतार लगा देता था — विकीपीडिया के लेख, न्यूज़ रिपोर्ट्स, ब्लॉग पोस्ट्स और क्वोरा की चर्चाएं.
गूगल खुद आपके सवाल का जवाब नहीं देता था. वह बस आपको दिखाता था कि जवाब कहां मिल सकता है, किसी मददगार लाइब्रेरियन की तरह.
लेकिन एआई आधारित टूल्स के आने के बाद यह मॉडल दबाव में आ गया. चैटजीपीटी जैसे टूल्स ने दिखा दिया कि लोग हमेशा वेबसाइट्स की लंबी लिस्ट नहीं चाहते. वे बिना इधर-उधर भटके अपने सवाल का सीधा, सुथरा, संक्षिप्त और समझदार जवाब चाहते हैं.
इसे सीधे शब्दों में कहें तो लोग अब लाइब्रेरियन नहीं, एक रिसर्च असिस्टेंट चाहते हैं. ऐसा असिस्टेंट जो खुद किताबें ढूंढे, फिर उन किताबों को छाने, और फिर उनसे निकला सार हमारे सामने रख दे.
खुद को ज़िंदा रखने के लिए गूगल ने भी अपना तरीका बदल लिया. अब उसके एआई ओवरव्यूज़ वही काम करते हैं, जो दूसरे एआई टूल्स करते हैं — यानी सवालों का फौरन जवाब देना. ऐसे में अक्सर यूज़र्स को लिंक पर क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती.
लेकिन इस प्रक्रिया में गूगल ने उन प्लेटफॉर्म्स को ही निगलना शुरू कर दिया है, जिन पर उसका सर्च इंजन टिका हुआ है — विकीपीडिया, क्वोरा, रेडिट और अनगिनत ब्लॉग्स और फोरम्स.
पहले अगर आप यह टाइप करते कि “टोक्यो में रहने का अनुभव कैसा है?”, तो क्वोरा की कोई चर्चा, विकीपीडिया का पन्ना या किसी स्वतंत्र वेबसाइट का लिंक सामने आता था. लेकिन अब पेज के सबसे ऊपर एक बढ़िया-सा एआई सारांश मिल जाता है. क्वोरा, रेडिट, विकीपीडिया और बाकी स्वतंत्र ब्लॉग्स के लिंक नीचे खिसक जाते हैं. कई बार ये लिंक्स हमें दिखते तक नहीं हैं.
इसका असर जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है.
क्वोरा और विकीपीडिया के लिए यह मुश्किल क्यों है?:
सबसे पहले बात करते हैं क्वोरा की. उसका पूरा मॉडल इसी पर टिका है कि लोग गूगल पर सवाल सर्च करें, क्वोरा के पन्नों तक पहुंचें, वहां दूसरों के व्यक्तिगत जवाब पढ़ें और चाहें तो अपना जवाब भी लिखें.
लेकिन गूगल से ट्रैफिक कम होने का मतलब है कम पाठक. पाठक कम होंगे तो जवाब देने वालों की संख्या भी घटेगी. इसका असर उस इंटरनेट कम्युनिटी पर पड़ेगा, जो क्वोरा के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है. ट्रैफिक कम होने का मतलब कम सब्सक्राइबर, कम विज्ञापन, और कम कमाई भी है.
क्वोरा को भी इसका एहसास है. इसी वजह से उसने अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म — ‘पो’ — शुरू किया है. लेकिन यह और भी उलझनभरी स्थिति है. क्वोरा जितना ज़्यादा एआई पर निर्भर होगा, उतना ही उसका पुराना कम्यूनिटी आधारित मॉडल कमजोर होता जाएगा. फिर वह भी बाकी एआई टूल्स की भीड़ में एक और टूल बनकर अपनी पहचान खो सकता है.
विकीपीडिया के सामने भी ऐसी ही — बल्कि इससे कहीं ज़्यादा पेंचीदा — चुनौती है. क्वोरा की तरह वह भी कंटेंट और कमाई (जो दान के ज़रिए आती है), दोनों के लिए अपने पाठकों पर ही निर्भर है. लेकिन जब एआई टूल्स सीधे-सीधे तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने लगें, या गूगल के एआई ओवरव्यूज़ की वजह से लोग विकीपीडिया पर ही न आएं, तो इससे न सिर्फ उसके ट्रैफिक पर असर पड़ता है, बल्कि बड़े पैमाने पर भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तैयार करने की उसकी क्षमता भी कमजोर होती है.
और विकीपीडिया का ढांचा ऐसा है कि वह खुद एआई टूल बन नहीं सकता. उसका ओपन, कम्युनिटी-आधारित और गैर-व्यावसायिक मॉडल एआई-जनित कंटेंट के लिए बना ही नहीं है.
लेकिन एआई की इस लहर को नज़रअंदाज़ करना भी मुमकिन नहीं है. भविष्य में जब बड़ी मात्रा में ऑनलाइन कंटेंट एआई से ही लिखा जाने लगेगा, तब विकीपीडिया के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि किसे भरोसेमंद स्रोत माना जाए और किसे नहीं. क्या तब वह एआई-जनित लेखों को भी स्रोत मानना शुरू कर देगा?
यह सवाल विकीपीडिया के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसकी पहचान ही इस बात पर टिकी है कि वह किसी जानकारी के लिए कितनी विश्वसनीय और प्रमाणित सूचनाओं का हवाला देता है.
और इंटरनेट का क्या?
लेकिन बात सिर्फ इन तीन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है. असली खतरा इंटरनेट के पूरे नॉलेज इकोसिस्टम की सेहत पर मंडरा रहा है.
सालों तक इंटरनेट एक अव्यवस्थित लेकिन जीवंत कंटेंट नेटवर्क बना रहा. बड़े न्यूज़रूम, यूनिवर्सिटीज़, जुनूनी ब्लॉगर, छोटे-छोटे फोरम और स्वतंत्र एक्सपर्ट इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थे. गूगल सर्च वह दरवाज़ा था, जो इन सबको लोगों के सामने लाने का काम किया करता था.
बेशक यह सिस्टम परफेक्ट नहीं था और इसमें एसईओ के खेल और क्लिकबेट या कमजोर कंटेंट की गड़बड़ियां थीं. लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से यह एक खुली व्यवस्था थी. अगर आपके पास कहने लायक कोई बात थी, तो आपके सुने जाने और खोजे जाने की गुंजाइश बनी रहती थी.
अब गूगल समेत अलग-अलग एआई टूल्स पर जो एआई सारांश दिखते हैं, वे जानकारी के इस बहाव को कुछ गिने-चुने बड़े और ‘आधिकारिक रूप से भरोसेमंद’ स्रोतों (सरकारी वेबसाइटें, बड़ी मीडिया संस्थाएं और अकादमिक पब्लिशर) तक समेट देने का खतरा पैदा कर रहे हैं.
इससे एसईओ पर टिका घटिया कंटेंट तो कमज़ोर पड़ेगा, जो बुरा नहीं है. लेकिन इसके साथ ही ईमानदारी से, सोच-समझकर लिखने वाले स्वतंत्र क्रिएटर्स का हौसला भी टूट सकता है. अगर लोग ऐसी सामग्री पढ़ना, देखना और उसका समर्थन करना छोड़ देंगे, तो फिर कोई ढंग का कुछ लिखेगा या रचेगा ही क्यों?
ऐसे में इंटरनेट एआई-जनित शोर-शराबे से भर सकता है. और इससे नुकसान सिर्फ यूज़र्स का नहीं, खुद एआई का भी होगा, जो अपनी ट्रेनिंग और बेहतर होने के लिए अच्छे और मौलिक इंसानी कंटेंट पर निर्भर है. और यह ख़तरा बहुत बड़ा है.
एक सेहतमंद इंटरनेट का मतलब सिर्फ जानकारी उपलब्ध होना नहीं है. इसका मतलब हर तरह की सामग्री और उस तक आसान पहुंच होना भी है. अगर एआई टूल्स इसी तरह बिना संदर्भों और स्रोतों वाला सारांश देते रहे, तो हम वह चीज़ ही खो देंगे जिसने इंटरनेट को अब तक एक कॉर्पोरेट और बंद जानकारियों वाले गढ़ में तब्दील होने से बचाकर रखा था.


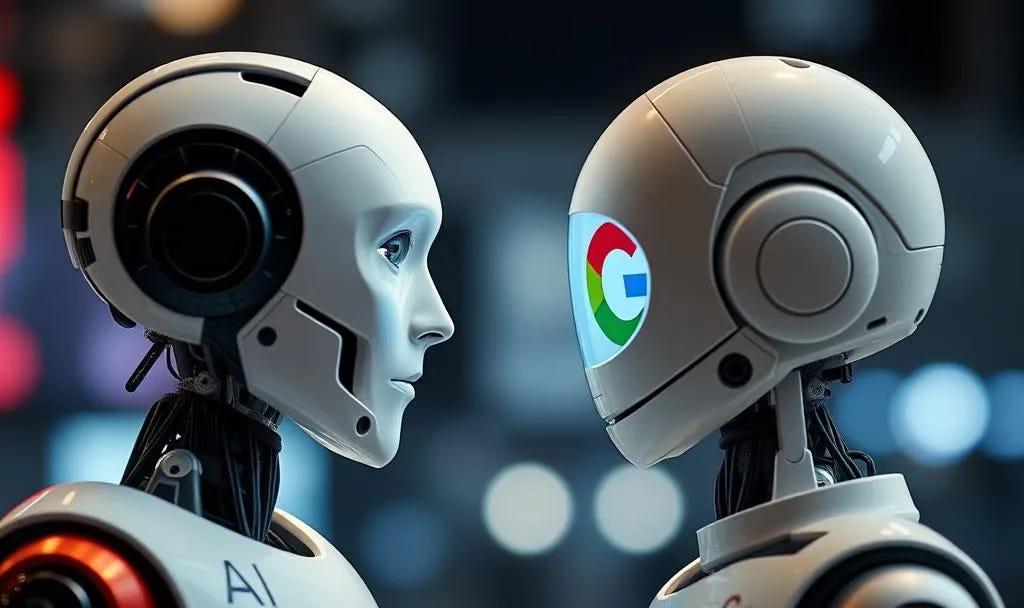
Thoughtful content, fresh ideas and enjoyable language will always be needed in all times.